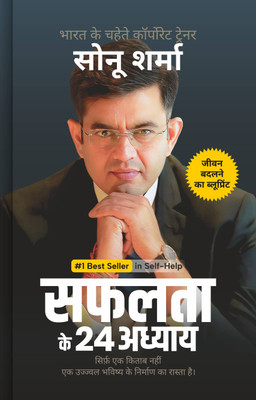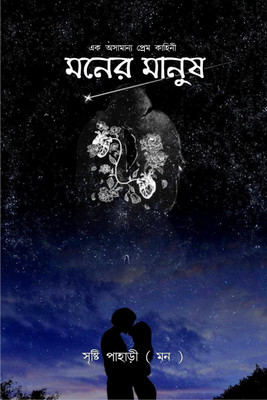Panchnama (Hindi, Hardcover, Jain Virendra)
Share
Panchnama (Hindi, Hardcover, Jain Virendra)
Be the first to Review this product
Special price
₹447
₹595
24% off
Available offers
T&C
T&C
T&C
T&C
Delivery
Check
Enter pincode
Delivery by19 Jan, Monday
?
View Details
Highlights
- Language: Hindi
- Binding: Hardcover
- Publisher: Vani Prakashan
- Genre: Fiction
- ISBN: 9789355187468
- Edition: 1st, 1996
- Pages: 290
Services
- Cash on Delivery available?
Seller
Description
पंचनामा -
अनाथ बेटे-बेटियों के परिवेश को अनाथ आश्रम के सन्दर्भ में रेखांकित करता यह उपन्यास 'पंचनामा' हालाँकि एक पारम्परिक और आदर्शवादी नायक की छवि ही प्रस्तुत करता है, लेकिन उपन्यास समाप्त होने से पहले बहुत दूर तक यह पंचनामा न तो किसी एक नायक का है और न किसी एक अनाथ का, बल्कि यह पंचनामा है उस समाज का जो अनाथ का दर्द नहीं समझ पाता; और है उस व्यवस्था का जिसने अनाथ आश्रम जैसी संस्थाओं को जन्म दिया है। उस प्रशासनिक ढाँचे का जो अनाथ आश्रमों का प्रबन्ध सम्भालता है।
इस सन्दर्भ में बहुत सारे सवाल उठते हैं। किसी भी आश्रम की पहली ज़रूरत क्या है— दया, कृपा, सहानुभूति अथवा स्रेह, आत्मीयता, बन्धुत्व और ममत्व? यह अहसास कि वह लाचार नहीं है या यह बोध कि वह हमेशा किसी दानी का शुक्रगुज़ार बना रहे? वह दो जून रोटी खाकर अपने पेट को शान्त कर ले और आँखों में भूख लिए फिरता रहे, या वह पाये कि जीवन का दूसरा नाम है स्वाभिमान और रोटी का मतलब है उसका हक़। उपन्यास में दसियों अनाथ बच्चे अपनी तमाम परिवेशगत अच्छाइयों, बुराइयों, शरारतों, नेकियों, शराफ़त, ग़ुस्से और प्यार के साथ अपनी तरफ़ ध्यान देने को बाध्य करते हैं। उन्हें अपनी नेकी के सिले की चिन्ता नहीं है, तो उद्दण्डता के प्रति कोई शर्मिन्दगी भी नहीं। वे अभाव से प्यार नहीं करते, अभाव में रह रहे हैं। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का यह उपहार हमारा सामना किस पीढ़ी से करवायेगा?
दरअसल, ये तमाम बातें कहने की नहीं, सोचने की हैं। और नयी पीढ़ी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार वीरेन्द्र जैन का यह उपन्यास सोचने का भरपूर अवसर अवश्य देता है।
Read More
Specifications
Dimensions
| Weight |
|
Book Details
| Imprint |
|
| Publication Year |
|
Contributors
| Author Info |
|
Be the first to ask about this product
Safe and Secure Payments.Easy returns.100% Authentic products.
Back to top